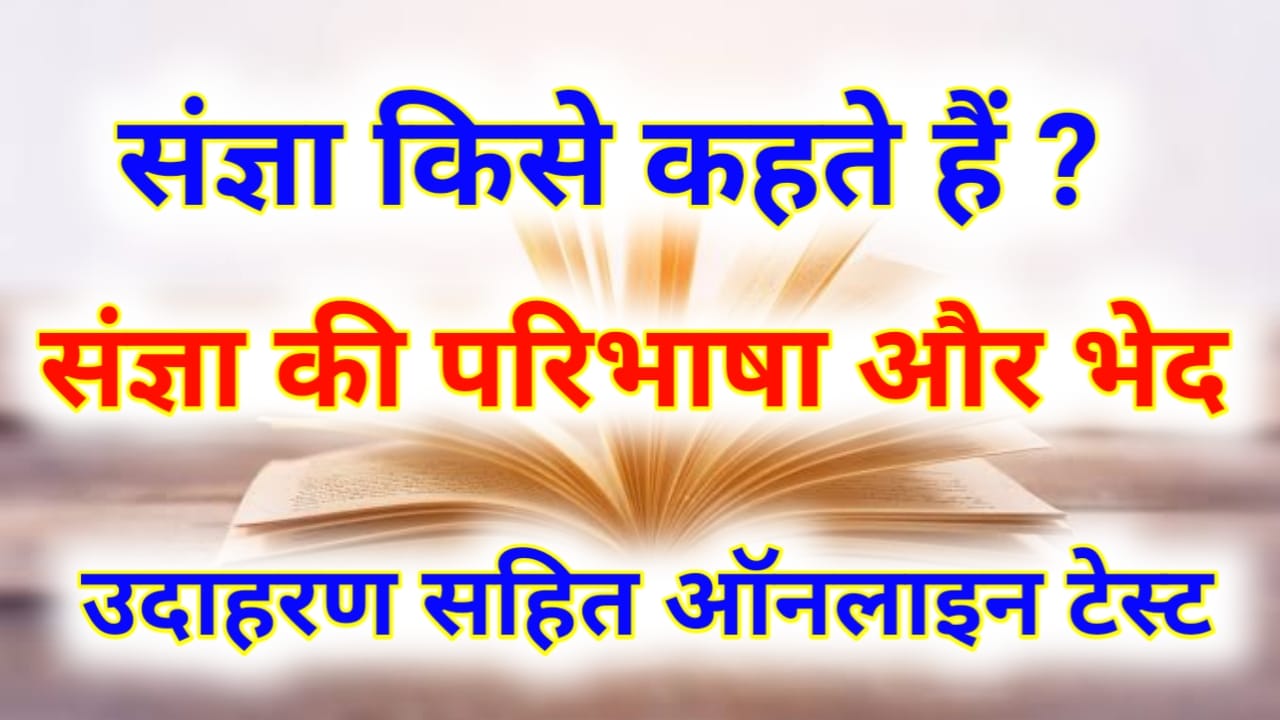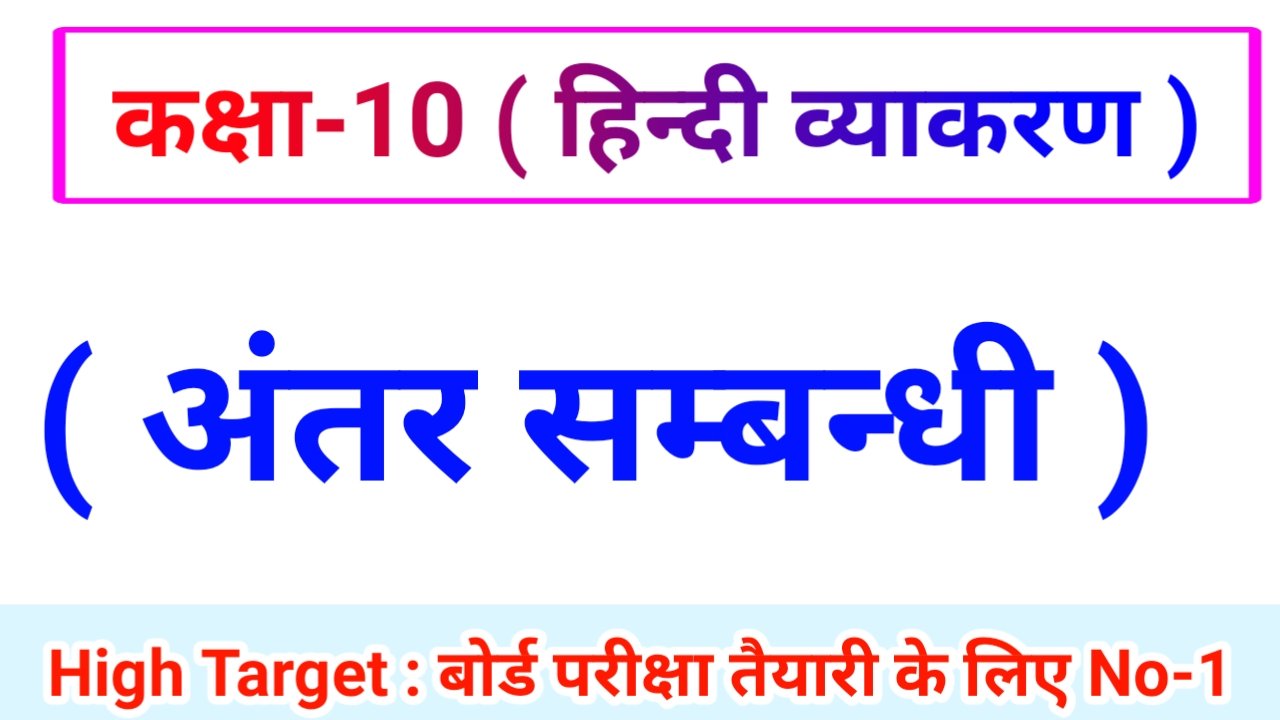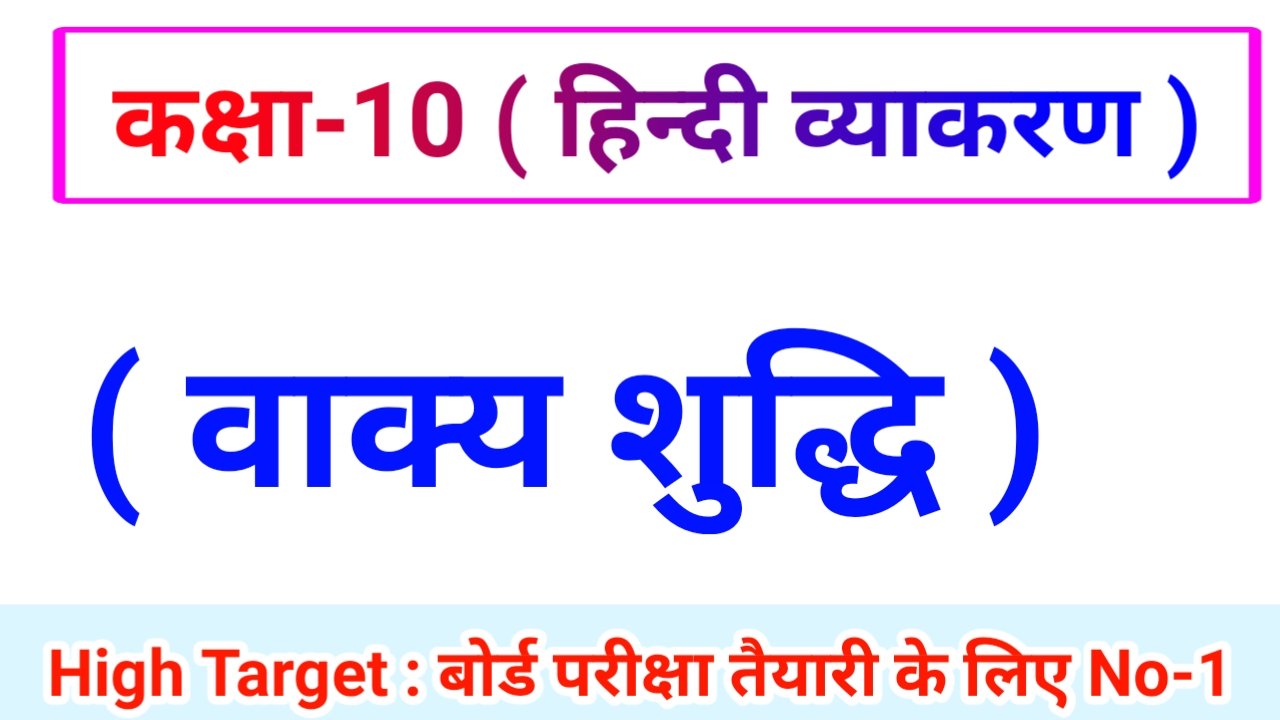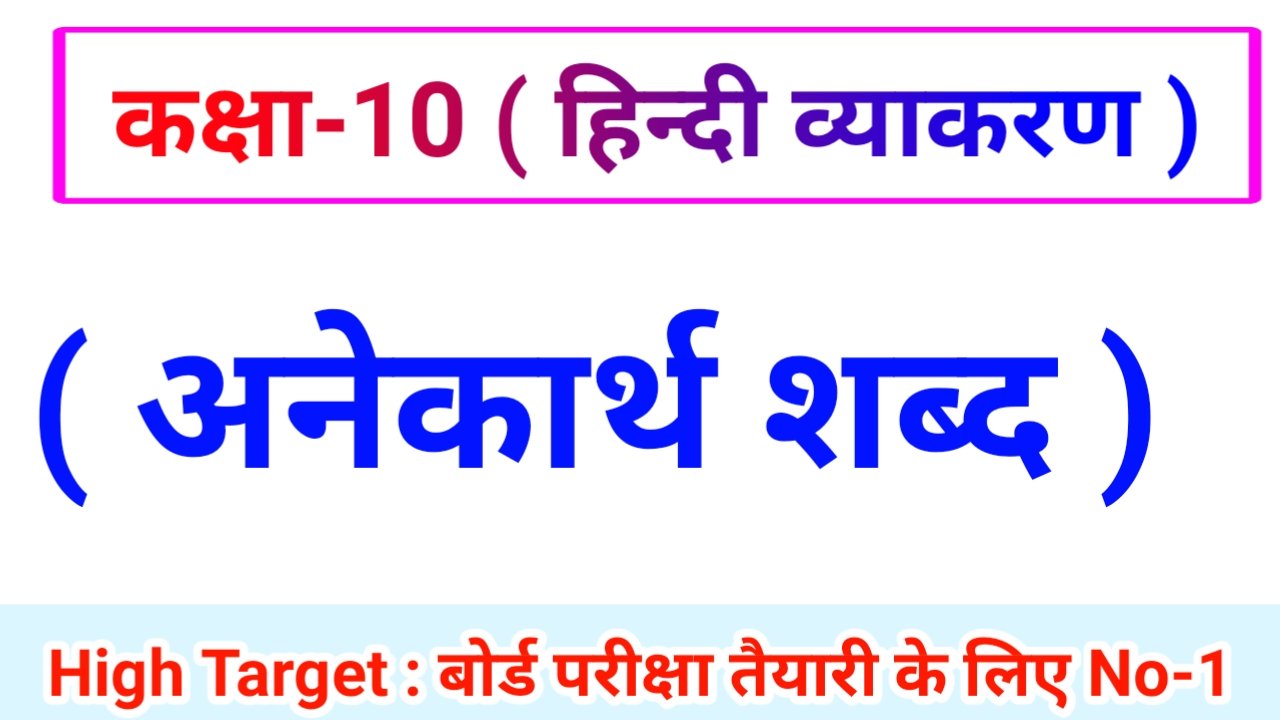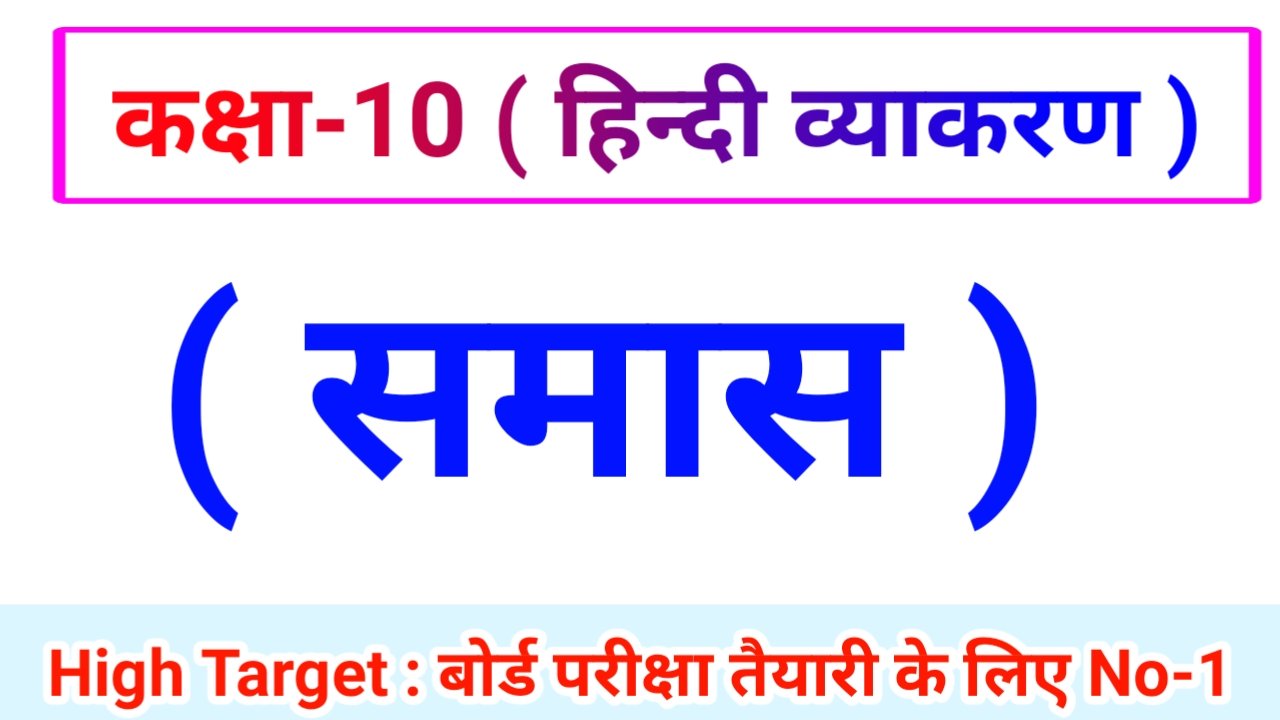
समास किसे कहते हैं? समास के भेद, उदाहरण सहित what is samas in hindi | Samas ke bhed ki paribhasha
| समास किसे कहते हैं? समास के भेद |
what is samas in hindi : समास क्या है ( samas in hindi ) ( vvi objective ) समास के कितने भेद हैं समास कितने प्रकार के होते हैं और समाज से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहां पर दिया गया है जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो अगर आप लोग समास की पूरी जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर दिया गया है। what is samas in hindi
समास क्या है ?
परिभाषा — दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है, उसे समस्तपद तथा इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा ‘और’ आदि अव्ययों का लोप हो जाता है।
समास की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं –
1. समास में दो पदों का योग होता है।
2. दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं।
3. दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है।
4. दो पदों में कभी पहला पद प्रधान और कभी दूसरा पद प्रधान होता है। कभी दोनों पद प्रधान होते हैं।
5. समास होने पर संधि भी हो सकती है, किन्तु ऐसा अनिवार्य नहीं है।
समास तथा संधि में अन्तर
समास तथा संधि में अन्तर — समास में दो पदों का योग होता है और संधि में दो वर्णों का। ये दोनों वर्ण भिन्न-भिन्न पदों के होते हैं। अतः, संधि होने पर दो वर्गों के संयोग से दोनों पद भी मिल जाते हैं । इस प्रकार समास वाले पदों में संधि और संधि वाले पदों में समास हो सकता है। जैसे—’पीताम्बर’ में दो पद हैं ‘पीत’ और ‘अम्बर’। संधि करने पर ‘पीत + अम्बर = पीताम्बर’ और समास करने पर ‘पीत है जो . अम्बर’ = ‘पीताम्बर’ होगा।
विशेष — संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, परन्तु समास हिन्दी शब्दों में भी होता है। अतः हिन्दी शब्दों में समासः करते समय संधि की आवश्यकता नहीं पड़ती।
संधि में वर्णों को तोड़ने की क्रिया को ‘विच्छेद’ कहते हैं और समास में पदों के तोड़ने की क्रिया को ‘विग्रह’ कहते हैं।
समस्तपद —दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को समस्तपद कहते हैं।
यथा – राजमार्ग दशानन
राजपुत्र यथाशक्ति
समासविग्रह – दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को पृथक् करना समास-विग्रह कहा जाता है।
यथा –
| समस्तपद | समास-विग्रह |
| माता-पिता | माता और पिता |
| राजमार्ग | राजा का मार्ग |
Samas ke kitne bhed hote hain
समास के कितने भेद हैं ?
समास निम्नलिखित छः प्रकार के होते हैं –
- द्वंद्व समास
- द्विगु समास
- कर्मधारय समास
- तत्पुरुष समास
- अव्ययीभाव समास
- बहुव्रीहि समास
द्वंद्व समास किसे कहते है उदाहरण सहित लिखें
| 1. द्वंद्व समास |
जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में बीच में और, तथा; अथवा, या आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा – समस्तपद – माता-पिता, विग्रह-माता और पिता आदि।
| समस्तपद | विग्रह |
| राम-लक्ष्मण | राम और लक्ष्मण |
| नमक-मिर्च | नमक और मिर्च |
| कृष्ण-बलराम | कृष्ण और बलराम |
| नर-नारी | नर और नारी |
| दाल-रोटी | दाल और रोटी |
| घी-शक्कर | घी और शक्कर |
| गुण-दोष | गुण और दोष |
| ऊँचा-नीचा | ऊँचा और नीचा |
| भला-बुरा | भला और बुरा |
| घर-द्वार | घर और द्वार |
| छोटा-बड़ा | छोटा और बड़ा |
| रोटी-कपड़ा | रोटी और कपड़ा |
| रात-दिन | रात और दिन |
| निशि-वासर | निशि और वासर |
| माँ-बाप | माँ और बाप |
| भीमार्जुन | भीम और अर्जुन |
| राजा-रंक | राजा और रंक |
| राधा-कृष्ण | राधा और कृष्ण |
| सुख-दुःखः | सुख और दुःख |
| वेद-पुराण | वेद और पराण |
द्विगु समास किसे कहते हैं?
| 2. द्विगु समास |
जिस समस्तपद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा जो किसी समुदाय की सूचना देता हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे –
| समस्तपद | विग्रह |
| पंचवटी | पाँच वटों का समूह |
| त्रिलोक | तीन लोकों का समूह |
| चौराहा | चार राहों का समाहार |
| अष्टाध्यायी | अष्ट (आठ) अध्यायों का समाहार |
| चतुर्वर्ण | चतुः (चार) वर्गों का समूह |
| पंचतत्त्व | पाँच तत्त्वों का समूह |
| नवग्रह | नौ ग्रहों का समाहार |
| चवन्नी | चार आनों का समूह |
| अठन्नी | आठ आनों का समूह |
| दुअन्नी | दो आनों का समूह |
| त्रिवेणी | तीन वेणियों का समाहार |
| चौमासा | चार मासों का समाहार |
| सप्तर्षि | सात (सप्त) ऋषियों का समूह |
| त्रिफला | त्रि (तीन) फलों का |
| समूह | शत (सौ) अब्दों (वर्षों) का समूह |
| त्रिभुवन | तीन (त्रि) भुवनों का समूह |
| सप्ताह | सप्त (सात) अहः (दिनों) का समूह |
| पंचमढ़ी | पाँच मढ़ियों का समूह |
| चौपाया | चार पायों वाला |
| तिपहिया | तीन पहियों वाली |
कर्मधारय समास किसे कहते हैं ?
| 3. कर्मधारय समास |
जिस समस्तपद के खण्ड विशेष्य-विशेषण अथवा उपमान उपमेय होते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यथा –
चन्द्रमुखी = चन्द्र (उपमान) + मुख (उपमेय)
लालमिर्च = लाल (विशेषण) + मिर्च (विशेष्य)
| कर्मधारय समस्तपद | विग्रह |
| चरण-कमल | कमलरूपी चरण |
| घनश्याम | घन के समान श्याम (काला) |
| काली टोपी | काली है जो टोपी |
| शुभागमन | शुभ है जो आगमन |
| लाल रूमाल | लाल है जो रूमाल |
| सज्जन | सत् (श्रेष्ठ) है जो जन |
| नील-कमल | नीला है जो कमल |
| नीलकंठ | नीला है जो कंठ |
| भीषण-प्रण | भीषण है जो प्रण |
| नरसिंह | सिंह के समान है जो नर |
| राजीव-लोचन | राजीव (कमल)रूपी लोचन (नेत्र) |
| नराधम | नर है जो अधम |
| पर्णशाला | पर्ण (पत्तों) से निर्मित है जो शाला |
| कमल-नयन | कमलरूपी नयन |
| मानवोचित | मानव के लिए है जो उचित |
| जन-गंगा | जनरूपी गंगा |
| वीरोचित | वीरों के लिए है जो उचित |
| कर-पल्लव | पल्लवरूपी कर |
| बुद्धिबल | बुद्धिरूपी बल |
| महाराज | महान है जो राजा |
| भवसागर | भवरूपी सागर |
| महारानी | महान है जो रानी |
| अल्पबुद्धि | अल्प है बुद्धि जिसके |
| महाशय | महान है जो आशय |
| इष्टमित्र | मित्र है जो इष्ट |
| पीताम्बर | पीत है जो अम्बर |
| पुरुषोत्तम | पुरुष है जो उत्तम |
तत्पुरुष समास किसे कहते हैं उदाहरण
| 4. तत्पुरुष समास |
जिस समस्तपद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक-चिह्न का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा –
| तत्पुरुष समस्तपद | विग्रह |
| राजकन्या | राजा की कन्या |
| जलमग्न | जल में मग्न |
| वातपीत | वात से पीत |
विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित छः भेद हैं
(क) कर्म तत्पुरुष
(ख) करण तत्पुरुष
(ग) सम्प्रदान तत्पुरुष
(घ) अपादान तत्पुरुष
(ङ) संबंध तत्पुरुष
(च) अधिकरण तत्पुरुष
(क) कर्म तत्पुरुष – इसमें कर्म कारक के विभक्ति-चिह्न ‘को’ का लोप होता है। यथा –
स्वर्गगत = स्वर्ग को गया हुआ
ग्रामगत = ग्राम को गया हुआ
(ख) करण तत्पुरुष – इसमें करण कारक के विभक्ति-चिह्न ‘से’ अथवा ‘द्वारा’ का लोप होता है। यथा –
रेखांकित = रेखाओं से (द्वारा) अंकित
गुणहीन = गुणों से हीन
(ग) सम्प्रदान तत्पुरुष – इसमें सम्प्रदान कारक की विभक्ति ‘के लिए’ का लोप होता है। यथा –
बलि-पशु = बलि के लिए पशु
मार्ग-व्यय = मार्ग के लिए व्यय
(घ) अपादान तत्पुरुष – इसमें अपादान कारक के विभक्ति-चिह्न ‘से’ लोप होता है । यथा –
धनहीन = धन से हीन
पथभ्रष्ट = पथ से भ्रष्ट
(ङ) संबंध तत्पुरुष – इसमें संबंध कारक के विभक्ति-चिह्न ‘का’, ‘की’ ‘के’ का लोप होता है। यथा –
विद्यार्थी = विद्या का अर्थी
कुलदीप = कुल का दीप
(च) अधिकरण तत्पुरुष – इसमें अधिकरण कारक के विभक्ति-चिह्न ‘में’ तथा ‘पर’ का लोप होता है। यथा –
व्याकरणपटु = व्याकरण में पटु
आप-बीती = आपपर बीती
तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद –
(क) नञ् तत्पुरुष समास – अभाव तथा निषेध के अर्थ में किसी शब्द (पद) से पूर्व ‘अ’ अथवा ‘अन्’ लगाकर जो समास बनता है, उसे नञ् तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा –
| समस्तपद | विग्रह |
| अधर्म | न + धर्म |
| अनिष्ट | अन् + इष्ट |
| अपूर्ण | न + पूर्ण |
| अनाचार | अन् + आचार |
| अनर्थ | न + अर्थ |
| अशिष्ट | न + शिष्ट |
| अमंगल | न + मंगल |
| अनुत्तीर्ण | अन् + उत्तीर्ण |
(संस्कृत के शब्दों के अतिरिक्त हिन्दी एवं उर्दू में भी निषेधार्थ में शब्द से पूर्व ‘अ’, ‘अन’, ‘अन्’ तथा ‘ना’, ‘गैर’ लगाकर बनाए गए शब्द (पद) नञ् तत्पुरुष
के अन्तर्गत आते हैं।)
| नञ तत्पुरुष शब्द | विग्रह |
| असम्भव | न + सम्भव |
| अनाश्रित | अन् + आश्रित |
| अकार्य | न + कार्य |
| अनर्थ | अन् + अर्थ |
| असुन्दर | अ + सुन्दर |
| अनहोनी | अन + होनी |
| नालायक | ना + लायक |
| गैरहाजिर | गैर + हाजिर |
(ख) अलुक् तत्पुरुष समास – जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद का विभक्ति का लाप नहीं होता, उसे अलुक् तत्पुरुष समास कहा जाता है। यथा –
| अलुक् तत्पुरुष शब्द | विग्रह |
| युधिष्ठिर | युधि (युद्ध में) स्थिर (टिकने वाला) |
| मृत्युंजय | मृत्युम् + जय (मृत्यु को जीतने वाला) |
| खेचर | खे + चर (आकाश में विचरण करने वाला) |
| सरसिज | सरसि + ज (तालाब में पैदा होने वाला) |
| मनसिज | मनसि + ज (मन में उत्पन्न होने वाला) |
(ग) उपपद तत्परुष – जिस समास में कोई उपपद हो तथा बाद म कृदन्त पद हो, उसे ‘उपपद तत्पुरुष’ कहते हैं।
| समस्तपद | विग्रह |
| जलज | जल में उत्पन्न (कमल) |
| मनोज | मन में उत्पन्न (कामदेव) |
| कुंभकार | कुंभ बनानेवाला |
| पंकज | पंक (कीचड़) में उत्पन्न |
अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं उदाहरण सहित
| 5. अव्ययीभाव समास |
जिस समास में प्रथम (पूर्व) पद अव्यय हो और जो उत्तरपद के साथ जुड़कर पूरे पद को अव्यय बना दे, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यथा-
| अव्ययीभाव समस्तपद | विग्रह |
| आमरण | मरणपर्यंत |
| आजन्म | जन्मपर्यंत |
| प्रतिदिन | दिन-दिन |
| बीचोबीच | बिल्कुल बीच में |
| साफ-साफ | बिल्कुल साफ |
| यथासमय | समय के अनुसार |
| यथा-शक्ति | शक्ति के अनुसार |
| यथासंख्या | संख्या के अनुसार |
| आजीवन | जीवनपर्यंत |
| यथाविधि | विधि के अनुसार |
| रातोंरात | रात-ही-रात में |
| प्रत्येक | एक-एक |
| घर-घर | प्रत्येक घर |
| भरपेट | पेट भरकर |
| आसमद्र | समद्रपर्यंत |
| बेखौफ | बिना डर के |
| बाकायदा | कायदे के अनुसार |
| हाथोहाथ | हाथ-ही-हाथ |
bahuvrihi samas examples in hindi
| 6. बहुव्रीहि समास |
जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वरन् दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा-शब्द के विशेषण होते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यथा –
| बहुव्रीहि समस्तपद | विग्रह |
| दशानन | दश हैं आनन जिसके अर्थात् रावण |
| त्रिलोचन | त्रि (तीन) हैं लोचन (नेत्र) जिसके अर्थात् शिव |
| चतुर्भुज | चतुः (चार) हैं भुजाएँ जिसकी अर्थात् विष्णु |
| लम्बोदर | लम्बा है उदर जिसका अर्थात् गणेश |
| पीताम्बर | पीत (पीला) है अम्बर जिसका अर्थात् विष्णु |
| चक्रपाणि | चक्र है पाणि (हाथ) में जिसके अर्थात् विष्णु |
| षडानन | षट् (छ:) हैं आनन जिसके अर्थात् कार्तिकेय |
| पंचानन | पंच (पाँच) हैं आनन जिसके अर्थात शिव |
| सहस्रबाहु | सहस्र हैं बाहु जिसकी अर्थात् दैत्यराज |
| द्विरद | द्वि (दो) हैं रद (दाँत) जिसके अर्थात् हाथी |
| मृत्युंजय | मृत्यु को जीतने वाला है जो अर्थात् शंकर |
| चन्द्रमुखी | चन्द्र के समान मुख वाली है जो (स्त्री) |
| नीलकंठ | नीला है कण्ठ जिसका अर्थात् शिव |
| गजानन | गज जैसा है आनन. जिसका अर्थात् गणेश |
| चन्द्रशेखर | चन्द्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव |
| तिमंजिला | तीन हैं मंजिलें जिसकी वह मकान |
| दिगम्बर | दिक् (दिशाएँ) हैं अम्बर (वस्त्र) जिसकी वह (नग्न |
| मृगनयनी | मृग जैसे नयनों वाली है जो (स्त्री) |
| मुगलोचनी | मृग जैसे लोचनों वाली है जो (स्त्री) |
| मेघना | मेघ जैसा है नाद जिसका वह अर्थात् रावण-पुत्र |
| इन्द्रजित | इन्द्र को जीतने वाला है जो अर्थात् मेघनाद |
| धर्मात्मा | धर्म में आत्मा है लीन जिसकी वह व्यक्ति |
| सुलोचना | सुन्दर लोचनों वाली है जो (स्त्री) |
| चारपाई | चार पाए हैं जिसके अर्थात् खाट |
| नीरज | नीर में जन्म लेने वाला है जो अर्थात् कमल |
| वारिज | वारि में जन्म लेने वाला है जो अर्थात् कमल |
| जलज | जल में जन्म लेने वाला है जो अर्थात् कमल |
| समास के सम्बन्ध में जानने योग्य बातें |
कुछ समासों में समानता प्रतीत होती है, किन्तु फिर भी उनमें अन्तर होता है।
जैसे-
(क) द्विगु और बहुव्रीहि समास में अन्तर – यद्यपि द्विगु समास में भी बहुव्रीहि समास की ही भाँति विशेषण-विशेष्य भाव पाया जाता है तथापि दोनों में पर्याप्त अन्तर है, क्योंकि द्विगु समास केवल संख्यावाचक विशेषण तक ही सीमित रहता है, जबकि बहुव्रीहि में ऐसा कुछ नहीं होता। द्विगु समास का अर्थ उसके शब्द-खंडों से भिन्न नहीं होता। जैसे—पंचवटी । इसमें पाँच वट-वृक्षों का समूह सूचित हो रहा है।
बहुव्रीहि समास में यदि पहला पद संख्यावाचक विशेषण बन आता है तो वह दूसरे पद का विशेषण न होकर दूसरे पद को भी साथ लेकर किसी अन्य(संख्या आदि) का विशेषण बन जाता है तथा उसका अर्थ उसके शब्दों के अर्थ से एकदम भिन्न होता है।
जैसे—’पंचानन’ (पंच + आनन) पाँच हैं आनन (मुख) जिसके अर्थात् सिंह। यहाँ बहुव्रीहि समास है।
(ख) कर्मधारय और बहुव्रीहि में अन्तर – कर्मधारय समास में समस्त पद में एक पद दूसरे पद का विशेषण या उपमान होता है। जैसे—’नीलांबर’ (नीला है जो आकाश) अर्थात् नीले रंग का अथवा ‘देहलता’ (देहरूपी लता) में ‘लता’ पद ‘देह’ पद का उपमान है।
बहुव्रीहि समास के दोनों पद किसी अन्य (संज्ञा आदि) पद के विशेषण होते हैं और इनका अर्थ शब्द-खंडों के अर्थ से सर्वथा भिन्न होता है । जैसे—’वज्रांगी’ वज्र के समान अंग हैं जिसके अर्थात् हनुमान। यहाँ ‘वज्र’ पद ‘अंगी’ पद का विशेषण न होकर दोनों ही पदों अन्य संज्ञा शब्द (हनुमान) के विशेषण हैं।
(ग) द्विगु और कर्मधारय में अन्तर — दोनों ही समासों के पदों में परस्पर विशेषण-विशेष्य भाव का संबंध पाया जाता है, किन्तु फिर भी अन्तर है –
द्विगु समास का पहला पद हमेशा ही संख्यावाचक विशेषण होता है, जबकि कर्मधारय में ऐसा नहीं होता अर्थात् कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक विशेषण कभी नहीं होता । जैसे –
नवरत्न – नौ रत्नों का समूह – द्विगु समास।
सज्जन – सत (अच्छा) है जो जन – कर्मधारय समास ।
| महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर |
* समास-विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए :
उत्तर ⇒
| शब्द | समास-विग्रह | समास |
| अकालपीड़ित | अकाल से पीड़ित | तत्पुरुष |
| अधपका | आधा पका हुआ | कर्मधारय |
| अन्न-जल | अन्न और जल | द्वंद्व |
| आजीवन | जीवनभर | अव्ययीभाव |
| कनकलता | सोने जैसी लता | कर्मधारय |
| गजानन | गज जैसा आनन है जिसका वह (गणेश) | बहुव्रीहि |
| गुरु-शिष्य | गुरु और शिष्य | द्वंद्व |
| चतुर्मुख | चार हैं मुख जिसके-ब्रह्मा | बहुव्रीहि |
| चक्रपाणि | चक्र है पाणि में जिसके वह | बहुव्रीहि |
| चौराहा | चार राहों का समूह | द्विगु |
| चरणकमल | कमल जैसे चरण | कर्मधारय |
| दानवीर | दान देने में वीर | तत्पुरुष |
| धनी-मानी | धनी और मानी नवग्रह नौ ग्रह | द्विगु |
| नीलकंठ | नीला है कंठ जिसका वह (शिव) | बहुव्रीहि |
| पंचानन | पाँच आनन का समूह | द्विगु |
| पाँच है | आनन जिसके वह (शिव) | बहुव्रीहि |
| भरपेट | पेट भरकर | अव्ययीभाव |
| भयभीत | भय से भीत | तत्पुरुष |
| मृगनयन | मृग जैसे नयन | कर्मधारय |
| मृगशावक | मृग का शावक | तत्पुरुष |
| मनगढ़त | मन से गढ़ी हुई | तत्पुरुष |
| मार्ग व्यय | मार्ग के लिए व्यय | तत्पुरुष |
| यथाशक्ति | शक्ति के अनुसार | अव्ययीभाव |
| यथाशीघ्र | जितना शीघ्र हो सके | अव्ययीभाव |
| राजपुत्र | राजा का पुत्र | तत्पुरुष |
| शोकाकुल | शोक से आकुल | तत्पुरुष |
| सालो-साल | अनेक साल | अव्ययीभाव |
| हस्तलिखित | हाथ से लिखित | तत्पुरुष |
| त्रिनेत्र | तीन हैं नेत्र जिसके वह (शिव) | बहुव्रीहि |
| त्रिफला | तीन फलों का समूह | द्विगु |
| त्रिभुवन | तीन भुवनों का समूह | द्विगु |
| प्रतिदिन | दिन-दिन | अव्ययीभाव |
| ऋणमुक्त | ऋण से मुक्त | तत्पुरुष |
* समस्त पद बताइए और समास का नाम भी दीजिए :
उत्तर ⇒
| शब्द | समस्त पद | समास |
| काम से पीड़ित | कामपीडित | तत्पुरुष |
| वंशी को धारण करता है जो | वंशीधर | बहुव्रीहि |
| रात ही रात में | रातोरात | अव्ययीभाव |
| राजा का पुत्र | राजपुत्र | तत्पुरुष |
| दिन-दिन | प्रतिदिन | अव्ययीभाव |
| जितना सम्भव हो | यथासम्भव | अव्ययीभाव |
| कमल के समान नयन | कमलनयन | कर्मधारय |
| आनंद में मग्न | आनंदमग्न | तत्पुरुष |
| तीन लोकों का समूह | त्रिलोक | द्विगु |
| शक्ति के अनुसार | यथाशक्ति | अव्ययीभाव |
| चार भुजाएँ हैं जिसकी | चतुर्भुज | बहुव्रीहि |
| गगन को चूमने वाला | गगनचुम्बी | बहुव्रीहि |
| घोड़ों की दौड़ | घुड़दौड़ | तत्पुरुष |
* समास किसे कहते हैं ?
उत्तर ⇒ दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है, उसे समस्त पद तथा उस प्रक्रिया को ‘समास’ कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा ‘और’ आदि अव्ययों का लोप हो जाता है ।
* समास के भेदों को उदाहरण सहित लिखें।
उत्तर ⇒ समास के छः भेद हैं :
(i) तत्पुरुष समास-जिस सामासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे-राजमंत्री, राजकुमार, राजमिस्त्री, राजरानी, देशनिकाला, जन्मान्ध, तुलसीकृत इत्यादि।
(ii) कर्मधारय समास – जिस सामासिक शब्द में विशेष्य-विशेषण और – उपमा-उपमेय का मेल हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं।जैसे-चन्द्र के समान मुख = चन्द्रमुख, पीत है जो अम्बर = पीताम्बर आदि।
(iii) द्विगु समास – जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड संख्याबोधक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं।
जैसे-दूसरा पहर = दोपहर, पाँच वटों का समाहार = पंचवटी, तीन लोकों का समूह = त्रिलोक, तीन कालों का समूह = त्रिकाल आदि।
(iv) द्वन्द्व समास – जिस सामासिक शब्द के सभी खंड प्रधान हों, उसे द्वन्द्व समास कहा जाता है। ‘द्वन्द्व’ सामासिक शब्द में दो पदों के बीच योजक चिह्न (-) भी रह सकता है। जैसे-गौरी और शंकर = गौरीशंकर। भात और दाल = भात-दाल। सीता और राम = सीता-राम। माता और पिता = माता-पिता इत्यादि।
(v) बहुव्रीहि समास – जो समस्त पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलावे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।
जैसे-जिनके सिर पर चन्द्रमा हो = चन्द्रशेखर (शंकर)। लम्बा है उदर जिनका = लम्बोदर (गणेशजी), त्रिशूल है जिनके पाणि में = त्रिशूलपाणि (शंकर) आदि।
(vi) अव्ययीभाव समास – जिस सामासिक शब्द का रूप कभी नहीं बदलता हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं।
जैसे – दिन-दिन = प्रतिदिन।
शक्ति भर = यथाशक्ति।
हर पल = प्रतिपल।
जन्म भर = आजन्म।
बिना अर्थ का = व्यर्थ आदि।
Hindi Grammer Question Answer